वैश्विक संशय के दौर में भी भारत-रूस की दोस्ती पक्की
रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे भारत आने की तैयारी

पुतिन के भव्य स्वागत के लिए भारत हो रहा तैयार
भारत-रूस संबंधों पर तैयार संदर्भ ग्रंथ पर दुनियाभर में चर्चा
अयांश गौरव सिंह
मास्को, 12 जुलाई। जैसे-जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष के अंत में 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए अपनी भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, दोनों देश अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नए प्रस्तावों को सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। यह उच्च-स्तरीय जुड़ाव ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर व्यापक परिवर्तन हो रहे हों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, आर्थिक बदलावों और बदलते रणनीतिक समीकरणों का पारंपरिक गठबंधनों पर प्रभाव पड़ रहा हो। इस पृष्ठभूमि में, भारत-रूस संबंध स्थायी विश्वास और व्यावहारिक सहयोग के एक आदर्श के रूप में उभर रहे हैं।
इस विकसित होती साझेदारी के केंद्र में एक आधारभूत स्तंभ निहित है, वह है आपसी विश्वास। यह विश्वास न केवल बदलती विश्व व्यवस्था की उथल-पुथल के बावजूद कायम रहा है, बल्कि हाल के वर्षों में और भी मजबूत हुआ है, क्योंकि दोनों देशों ने रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता पर आधारित विदेश नीतियों का अनुसरण किया है। नई दिल्ली और मॉस्को के लिए, यह साझेदारी अब केवल द्विपक्षीय एजेंडों तक सीमित नहीं है। यह व्यापक अंतरराष्ट्रीय ढांचों के भीतर एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है। भारत-रूस संबंधों की वर्तमान गतिशीलता और भविष्य की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और व्यक्त करने के लिए, दोनों देशों के विद्वानों और पेशेवरों के एक समूह ने भारत और रूस: एक परिवर्तनकारी युग में स्थायी विश्वास (इंडिया एंड रशिया : इंड्योरिंग ट्रस्ट इन ए ट्रांसफॉरमेशनल एरा) नामक एक नव प्रकाशित ग्रंथ में योगदान दिया है। यह ग्रंथ भारत-रूस संबंधों के संपूर्ण आयामों (स्पेक्ट्रम) को लेकर रक्षा और ऊर्जा जैसे विरासत क्षेत्रों एवं उच्च प्रौद्योगिकी और जलवायु सहयोग जैसे उभरते क्षेत्रों तक तमाम विषद एवं विस्तारित दृष्टिकोणों का एक समृद्ध संकलन प्रस्तुत करता है।
इस पुस्तक का संपादन डॉ. लिडिया कुलिक ने किया है, जो भारत मामलों की एक प्रमुख रूसी विशेषज्ञ और मॉस्को स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कोल्कोवो में भारत अध्ययन विभाग की प्रमुख हैं। वह रूसी विज्ञान अकादमी के प्राच्य अध्ययन संस्थान में वरिष्ठ शोध अध्येता भी हैं। एक साक्षात्कार में, डॉ. लीडिया कुलिक ने इस बात पर जोर दिया कि यह पुस्तक द्विपक्षीय संबंधों पर, विशेष रूप से हाल के वर्षों में सामने आए गहन वैश्विक परिवर्तनों के आलोक में, एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह संस्करण रूस और भारत के विचारों का एक संग्रह है जो उन संबंधों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जो हमारी दोनों सभ्यता के लोगों के साथ-साथ गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ सोवियत काल से लेकर 2024 के ऐतिहासिक वर्ष तक, भारत-रूस संबंधों की ऐतिहासिक यात्रा को समाहित करती है। परस्पर संबंधों की इस यात्रा ने रिश्तों में अभूतपूर्व उत्थान एवं प्रगाढ़ता देखी है।
ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के निर्माण के योगदानकर्ताओं में रणनीतिक थिंक टैंक नैटस्ट्रैट के संयोजक और रूस में भारत के पूर्व राजदूत पंकज सरन भी शामिल रहे हैं। सरन द्विपक्षीय संबंधों की खूबियों, कमजोरियों और भविष्य के दृष्टिकोण का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करते हैं। पश्चिम के साथ रूस के टकराव और चीन के साथ उसके बढ़ते गठजोड़ जैसी चुनौतियों के बावजूद, उनका निष्कर्ष है कि भारत-रूस संबंध अपने गहन संस्थागत स्वरूप और परस्पर जुड़े रणनीतिक हितों के कारण मजबूत बने रहेंगे।
ग्रंथ में बार-बार और कई अध्यायों में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का उल्लेख आता है। यह ऐसा दृष्टिकोण है, जिसे मास्को बहुत महत्व देता है। मास्को स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में भारतीय अध्ययन केंद्र की प्रमुख और पद्मश्री पुरस्कार विजेता तात्याना शौम्यान कहती हैं कि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष और स्वतंत्र बने रहने की उसकी इच्छा से आकार लेती है। इसी नीति के तहत भारत ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों पर चिंता भी व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र में रूस-विरोधी प्रस्तावों से दूर रहकर पश्चिमी लाइन पर चलने से इन्कार भी कर दिया। शौम्यान बताती हैं कि कैसे भारत अपनी विदेश नीति का लगातार वैश्वीकरण कर रहा है और न केवल दक्षिण एशिया में, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी बड़ी भूमिका तलाश कर रहा है। जैसे-जैसे भारत की आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमताएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नियम-निर्माता बनने की उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही है। भारत ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और रूस-भारत-चीन (आरआईसी) वार्ता जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भी भारत-रूस सहयोग को रेखांकित करता है। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, फिर भी ऐसे मंच प्रभाव बढ़ाने और समन्वय को गहरा करने की महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करते हैं।
जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा के महत्व पर भी ग्रंथ में प्रकाश डाला गया है। पुनर्निर्वाचन के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा और 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद उनकी पहली रूस यात्रा को खास तौर पर रेखांकित किया गया है, क्योंकि वह समय अत्यंत महत्वपूर्ण था। इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ दि रशियन एकेडेमी ऑफ साइंसेज (इमेमो-रास) में इंडो-पैसिफिक केंद्र की रिसर्च फेलो लेयला तुरायानोवा के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री की उस रूस यात्रा ने पश्चिम के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हुए भी अपनी पारंपरिक साझेदारियों को बनाए रखने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त किया। उनका तर्क है कि भारत-रूस संबंध यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न तनाव की परीक्षा में सफल रहे हैं और विशेष रूप से व्यापार और संपर्क के क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ उभरे हैं।
कनेक्टिविटी वास्तव में चर्चा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तीन लेखकों, रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद से जुड़ी जूलिया मेलनिकोवा, अर्बातोव संस्थान की नतालिया वियाखिरेवा और आरआईएसी के कार्यक्रम समन्वयक ग्लीब ग्रिजलोव ने इस बात पर गहन शोध किया है कि कैसे भारत रूस के परिवहन और बुनियादी ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी से शामिल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी), आर्कटिक शिपिंग और उत्तरी समुद्री मार्ग, सभी को एक ऐसे विश्व में सहयोग के प्रमुख स्तंभों के रूप में पहचाना जाता है जहां आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार मार्गों का तेजी से पुनर्संयोजन किया जा रहा है।
रूस की प्रमुख पेट्रोकेमिकल कंपनी सिबुर के अधिकारी सर्गेई कोमिशान ने आर्थिक सहयोग का और विश्लेषण किया है। वे द्विपक्षीय औद्योगिक सहयोग की व्यावसायिक संभावनाओं को दर्शाने के लिए रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स, जो एक सफल भारत-रूस संयुक्त उद्यम है, का उदाहरण देते हैं। वे राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के एकीकरण, जल पुनर्चक्रण (रिसाइकलिंग) तकनीकों में सहयोग और एक संयुक्त कार्बन क्रेडिट ढांचे सहित नए अवसरों की ओर भी इशारा करते हैं। रक्षा और सामरिक सहयोग भारत-रूस साझेदारी का एक ऐतिहासिक आधार रहा है। यह अब भी प्रासंगिक बना हुआ है, लेकिन इसमें बदलाव भी आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्लेषक आर्यमन निझावन इस बात पर शोध करते हैं कि यूक्रेन संघर्ष से मिले सबक भविष्य के सैन्य-तकनीकी सहयोग को कैसे आकार दे सकते हैं। ड्रोन तकनीक, ड्रोन-रोधी प्रणालियां और यहां तक कि सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों को संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए आशाजनक क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हालांकि एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, संरचित सहयोग के अभाव से ग्रस्त है। इमेमो-रास की ओल्गा उस्त्युजंतसेवा और इवान डैनिलिन का तर्क है कि इस क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग का भविष्य राज्य-संचालित मॉडलों से आगे बढ़कर निजी क्षेत्र की भागीदारी की ओर बढ़ने के संकेत दे रहा है। दोनों शोधकर्ता भारत और रूस दोनों देशों में स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल और एसएमई-नेतृत्व वाले नवाचार की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हैं और बेहतर संस्थागत ढांचे और निरंतर निवेश की आवश्यकता पर बल देते हैं।
रूस के वरिष्ठ बैंकर और पूर्व उप-वित्त मंत्री सर्गेई स्टोर्चैक, द्विपक्षीय संबंधों के वित्तीय आयामों पर चर्चा करते हैं। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसकी अर्थव्यवस्था का तेजी से गैर-डॉलरीकरण हो रहा है, ऐसे में भारत स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के प्रयोग और सुरक्षित, तेज वित्तीय संदेश प्रणाली स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है। एमजीआईएमओ की अन्ना किरीवा, आसियान और हिंद-प्रशांत के व्यापक संदर्भ में भारत-रूस संबंधों का विश्लेषण करती हैं। वह नीतिगत संवादों, तीसरे बाजारों के लिए संयुक्त हथियार उत्पादन, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सहयोगी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों सहित, जुड़ाव के नए प्रारूपों का प्रस्ताव करती हैं। उनका विश्लेषण एक व्यापक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है क्योंकि दोनों देश अपने कूटनीतिक उपकरणों और क्षेत्रीय साझेदारियों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के अलेक्सी जखारोव इस बात पर जोर देते हैं कि रूस का क्षेत्रीय दृष्टिकोण विस्तृत हो रहा है। जहां भारत रूस की दक्षिण एशिया रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है, वहीं मॉस्को अपनी बढ़ती कमजोरियों को संतुलित करने और अपने राजनयिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ तेजी से जुड़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भारत और रूस के मजबूत संबंधों पर प्रकाशित ग्रंथ दुनिया की सबसे समय-परीक्षित (टाइम-टेस्टेड) द्विपक्षीय साझेदारियों का सामयिक और गहन अन्वेषण प्रस्तुत कर रहा है। बदलती वैश्विक गतिशीलता के साथ, दोनों देशों ने दिखाया है कि उनका संबंध केवल शीत युद्ध काल का अवशेष नहीं है, बल्कि एक गतिशील, दूरदर्शी गठबंधन है जो 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुकूल ढलने में सक्षम है। ऊर्जा और रक्षा से लेकर कनेक्टिविटी और डिजिटल नवाचार तक, भारत-रूस साझेदारी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है।
#पुतिनभारतआगमन, #भारतरूसमित्रता, #वैश्विकसंशय, #विश्र्वनीति, #StrategicPact


9.jpg)
4.jpg)
2.jpg)

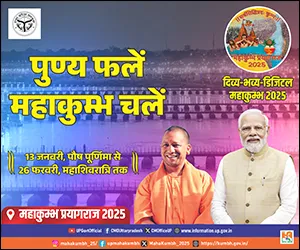
2.jpg)

6.jpg)

6.jpg)
