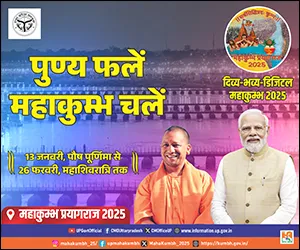जनता को उसकी भाषा में न्याय मिलना चाहिए
अंग्रेजों की गुलामी से मानसिक तौर पर भी मुक्त होने की जरूरत
.jpg)
डॉ. मोतीलाल गुप्ता आदित्य
संविधान निर्माण के समय जो भी स्थितियां या कारण रहे हों, मैं समझता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 348 जनतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। किसी भी देश में वहां के नागरिकों को उस देश की भाषा में न्याय तो मिलना ही चाहिए। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा अपवाद होगा जहां के न्यायालयों में वहां के लोगों को उसे देश की भाषा में न्याय न मिलता हो। संविधान का अनुच्छेद 348 हमें आज भी अंग्रेजों की गुलामी का एहसास करवाता है। संविधान का यह अनुच्छेद देश की जनता को उसकी भाषा में न्याय से वंचित करता है।
अदालत में किसी व्यक्ति का मुकदमा चल रहा है और उसे पता न हो कि उसका वकील क्या कह रहा है, न्यायाधीश क्या कह रहा है और निर्णय क्या हो रहा है? जो न्यायपालिका उसे गूंगा और बहरा बना दे, उसे न्याय कैसे कहा जा सकता है? उसे सही कैसे ठहराया जा सकता है? ऐसी स्थिति तो राजा महाराजाओं के समय में भी नहीं थी। संविधान के अनुच्छेद 348 की व्यवस्था अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के अनुकूल हो सकती है पर जनता के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। यह अत्यंत आवश्यक है कि जिस व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की गई है या इसके विरोध याचिका दायर की गई है उसे पता लगना चाहिए न्यायालय में क्या हो रहा है। उसे अपनी बात न्यायालय में रखने का अधिकार भी होना चाहिए, जो उसकी भाषा में ही संभव है।
यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, देश की जनता संविधान के लिए नहीं है, बल्कि भारत का संविधान जनता के हित के लिए है। यही संविधान संसद को जनहित के लिए आवश्यकतानुसार संविधान संशोधन की शक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 348 को संशोधित करते हुए इसमें संविधान के अनुच्छेद 350 के उपबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति व्यथा निवारण के लिए देश के किसी भी हिस्से में संघ में और उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा में अपना आवेदन या अभ्यावेदन दे सकता है। ठीक यही बात देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में भी होनी चाहिए।
अंग्रेजी, जो कि औपनिवेशिक भाषा है, यानी अंग्रेजों की गुलामी की भाषा है, जो भारत के नागरिकों की ही भाषा नहीं है, जो संविधान की अष्टम अनुसूची में भी नहीं है, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में उस भाषा में न्याय की अनिवार्यता की बात को किसी भी तरह जनतंत्र के अनुकूल नहीं माना जा सकता। यदि अंग्रेजी को रखना भी है तो वैकल्पिक भाषा के रूप में रखा जा सकता है।
अब आते हैं दूसरी बात पर। संविधान के अनुच्छेद 348 (2) में उपबंध है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि ऐसा निर्णय करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य की सहमति ली जाए। लेकिन आगे चलकर संविधान के अनुच्छेद 348 में भारत की जनता को प्राप्त इस अधिकार मैं भी एक पेंच फंसा दिया गया।
1965 की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक 21 मई 1965 को आयोजित की गई थी। उसमें संविधान के अनुच्छेद 348 के प्रतिकूल निर्णय लिया गया। उनके निर्णय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया, The Cabinet Committees decision dated 21.05.1965 has stipulated that consent of the Chief Justice of India be obtained on any proposal relating to use of a language other than English in the High Court. अर्थात अगर कोई राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा (जैसे हिंदी या राज्य की क्षेत्रीय भाषा) का प्रयोग करने हेतु अनुच्छेद 348 (2) के अंतर्गत प्रस्ताव भेजती है, तो केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को मंजूर करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है।
यहां यह प्रश्न उठता है कि जो बात भारत के संविधान में है ही नहीं, उसे क्यों लाया गया? प्रारंभ में राजस्थान (1950), उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में भाषा परिवर्तन के प्रस्ताव इसी प्रक्रिया के तहत मंजूर किए गए थे। लेकिन फिर इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। क्योंकि सरकार के 1965 के निर्णय के अनुसार किसी राज्य से आए प्रस्ताव के लिए पहले सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक है और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव पर सहमति ही नहीं। जब सूचना का अधिकार के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से जानकारी मांगी तो यह सूचित किया गया, विभाग में पश्चिम बंगाल, मद्रास, गुजरात, छत्ती
जो हुआ वह जनभाषा में न्याय के अधिकार की हत्या के समान था। जनभाषा में न्याय को लेकर इससे तत्कालीन सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि 60 साल पहले के तत्कालीन सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय को हम अब क्यों नहीं बदल पा रहे? जनभाषा में न्याय को लेकर हम कब तक पिछली सरकार को कोसते रहेंगे। अब जबकि भारत के गृहमंत्री ने यह कहा है कि अब हम ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं कि भारत में अपनी भाषा बोलने वालों को नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी तो मैं समझता हूं कि जनभाषा में न्याय के इस बंद दरवाजे को खोलने का इससे उत्तम समय क्या हो सकता है।
इस मौके पर हमें राष्ट्रपति के 1960 के आदेशों का भी संज्ञान ले लेना चाहिए, जिनमें यह कहा गया है, उच्चतम न्यायालय अन्ततः अपना सब काम हिंदी में करे, यह सिद्धांत रूप में स्वीकार्य है और इसके संबंध में समुचित कार्यवाही उसी समय अपेक्षित होगी जब कि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगा। जैसा कि आयोग की सिफारिश की तरमीम करते हुए समिति ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में यह व्यवस्था करने के लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करे कि निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिंदी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा।
अब जबकि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व कई न्यायाधीशों ने और वर्तमान न्यायाधीशों ने भी जनभाषा में न्याय की आवश्यकता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है तो अब कोई ऐसा कारण प्रतीत नहीं होता कि देश की जनता के लिए जनभाषा में न्याय का मार्ग न खोला जा सके।
#भाषाईन्याय, #जनताकाभाषामेंन्याय, #भाषाईसमानता, #भाषाईपहचान, #न्यायसभीकेलिए, #मातृभाषान्याय, #न्यायिकसमावेशिता


.jpg)