हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की नीति और राजनीति
14 सितंबर हिंदी दिवस पर विशेष : स्वतंत्रता संग्राम से अब तक…
4.jpg)
डॉ. मोतीलाल गुप्ता ‘आदित्य’
हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात जो कुछ हुआ है, वह अपने आप में एक लंबी और पेचीदा कहानी है। समय-समय पर तत्कालीन सरकारों ने जो नीति बनाई और अपनाई, क्या उसका पालन हुआ? जो संकल्प लिए गए, क्या उन्हें पूरा किया गया? बात हिंदी और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की होती रही, लेकिन अंग्रेजी कैसे आगे बढ़ती गई, इस पर भी विमर्श किया जाना चाहिए। यह विचार-विमर्श इसलिए भी जरूरी है कि मौजूदा भारत सरकार ने जो भाषा-नीति अपनाई है, वह एक बड़े परिवर्तन का संकेत देती है।
स्वतंत्रता-संग्राम के दौर में सभी अहिंसावादी और क्रांतिकारी, सभी स्वतंत्रता-सेनानियों, और महापुरुषों ने एक स्वर में यह विचार रखा था कि देश का काम राज्यों में राज्यों की भाषा में हो और राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया जाए, जिसे राष्ट्रभाषा कहा गया। राष्ट्रभाषा के रूप हिंदी ने स्वतंत्रता-संग्राम में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। इसी के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदी के प्रचार-प्रसार की संस्थाएं स्थापित की गईं ताकि स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क के लिए राष्ट्रभाषा के माध्यम से व्यवहार किया जा सके। इस कार्य में महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका थी।
लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात परिदृश्य बदल गया। संविधान सभा राष्ट्रभाषा के स्थान पर राजभाषा शब्द स्थापित हो गया। राज्यों में राज्य की राजभाषा और देश के स्तर पर देश की, अर्थात संघ की राजभाषा की बात हुई। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो सारा मामला सरकारी कामकाज की भाषा तक सिमट कर रह गया। जहां स्वाधीनता के समय एक प्रतिशत लोग भी अंग्रेजी में प्रवीण नहीं थे और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कुछ बड़े महानगरों में अति धनाढ्य लोगों तक सीमित थे। सामान्य जन तो अपने राज्य की भाषा में ही पढ़ता था, उसे तो यह भी पता न था कि अंग्रेजी माध्यम के भी विद्यालय होते हैं। लेकिन आगे चलकर ऐसी नीतियां अपनाई गई कि नर्सरी तक और गांव-गांव तक अंग्रेजी माध्यम पहुंच गया।
यह भी सर्वविदित है कि तमाम विवादों के बावजूद अंततः हिंदी को राजभाषा का पद तो दिया गया लेकिन वह भी आधा-अधूरा। संविधान लागू होने के बाद पहले 15 साल के लिए अंग्रेजी को स्थापित किया गया और फिर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित- 1967) के माध्यम से हिंदी के साथ अंग्रेजी को अघोषित राजभाषा के रूप में भी स्थापित कर दिया गया। सच तो यह है कि अंग्रेजी मुख्य राजभाषा बन गई और हिंदी सह-राजभाषा बन कर रह गई। जहां हिंदी केवल संघ की और कई राज्यों की राजभाषा है, वहीं अंग्रेजी भारत संघ की अघोषित राजभाषा होने के साथ-साथ भारत के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की अघोषित राजभाषा भी बना दी गई। इसी के साथ-साथ विभिन्न कानूनों के अंतर्गत दी जाने वाली सूचनाओं की भाषा तय न करने के कारण, वहां अंग्रेजी स्थापित हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जो स्थान हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मिलना था, उस स्थान पर धीरे-धीरे अंग्रेजी ने अपना कब्जा जमा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी भारत संघ और भारत के राज्यों के साथ-साथ न्याय, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में स्थापित कर दी गई। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया। संविधान की अष्टम अनुसूची में जो अंग्रेजी है ही नहीं, उसे पिछले दरवाजे से लाकर भारत की तथा भारत के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की भाषा के साथ-साथ अंतरराज्यकीय संपर्क की भाषा भी बना दिया गया। बात संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी की होती रही और राज अंग्रेजी का चलने लगा। यह जो कुछ हुआ, वह निश्चय ही सरकार की सोची-समझी रणनीति के तहत ही हुआ।
संविधान के अनुच्छेद 348 (1) में तो अंग्रेजी को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की और विधि भाषा बना दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 348 (2) मैं राज्यों के उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी और राज्यों की राजभाषा अपनाने का जो दरवाजा रखा गया था। 1965 में उसे भी असंवैधानिक रूप से एक मंत्रिमंडलीय निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जब किसी राज्य के राज्यपाल नें अपने राज्य स्थित उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अंतर्गत अपने राज्य की राजभाषा की मांग की तो सरकार ने उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे नकार दिया। इस तरह तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हरियाणा राज्यों के प्रस्ताव आज भी सरकारी फाइलों में धूल खा रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी कहने को भारत संघ की और कुछ राज्यों की राजभाषा रही, लेकिन अंग्रेजी का साम्राज्य संघ से लेकर राज्यों तक, विधि से न्याय तक और शिक्षा से लेकर व्यापार-व्यवसाय तक हर क्षेत्र में ऊपर से नीचे तक पसर गया। अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भी कमोबेश ऐसा ही हुआ।
1986 की शिक्षा नीति के पश्चात भारत में स्कूली शिक्षा का तेजी से अंग्रेजीकरण होने लगा था। इस समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा में अंग्रेजी को बढ़ाने के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए कहा गया कि हमें भूल जाना चाहिए की अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। भारत में विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर अंग्रेजी को अपनाए जाने की और सभी शिक्षकों को अंग्रेजी में दक्ष बनाए जाने की आवश्यकता है। फिर जब ज्ञान आयोग बना तो उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने खुलकर भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी की वकालत की। भारत की राजधानी दिल्ली में भी 1986 और उसकी कई वर्षों बाद तक स्नातक स्नातकोत्तर तक की शिक्षा हिंदी में उपलब्ध थी। राज्यों में भी स्कूली शिक्षा तो लगभग पूरी तरह वहां की भाषाओं में उपलब्ध थी। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाले ज्ञान आयोग की सिफारिशें भी अंग्रेजी के पक्ष में थीं। उसके बाद जिस गति से अंग्रेजी को बढ़ाया गया, नर्सरी स्तर तक अंग्रेजी माध्यम पहुंच गया। महानगरों, नगरों और कस्बों से होते हुए अंग्रेजी माध्यम गांव-गांव तक पसर गया। सबको लगने लगा कि उच्च शिक्षा और उच्च रोजगार अंग्रेजी से ही मिल सकता है। व्यवस्था में तमाम परिवर्तनों के चलते, यही हुआ भी। इसका परिणाम यह हुआ कि मातृभाषा माध्यम में केवल वही विद्यार्थी रह गए जो महंगे अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते थे। आज भी भारत में कमोबेश यही स्थिति है।
उधर वोट बैंक की राजनीति भी हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के प्रयोग व प्रसार में बाधा बन कर खड़ी रही। स्वतंत्रता पूर्व जहां राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात थी। बाद में हिंदी विरोध को राजनीति का औजार बना दिया गया। तमिलनाडु सहित कर्नाटक, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में भी कमोबेश हिंदी के विरुद्ध विषवमन होता रहा है। इनमें से कुछ की आपत्ति यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाए, हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों न कहा जाए , या फिर यह कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है।
देखा जाए तो स्वतंत्रता पूर्व से लेकर अब तक अगर किसी एक बात पर सहमति रही है, तो वह त्रिभाषा-सूत्र। यही बात राजभाषा संकल्प-1968 में त्रिभाषा सूत्र में निहित है। भले ही उसके कार्यान्वयन में कुछ अंतर हो। समानता यह कि पहले राज्य की भाषा, फिर देश की भाषा और विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी। कमोबेश देश में यही चलता भी रहा है। यह बात अलग है कि राजनीतिक कारणों से कुछ राज्यों में इसका विरोध भी किया गया। यही नहीं, राजनीतिक वर्चस्व की आकांक्षा के चलते हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी की बोलियों और हिंदी के बीच भी संघर्ष पैदा किया गया। हिंदी की अनेक बोलियों के स्वयंभु ठेकेदारों ने इन्हें हिंदी के समकक्ष संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने की मांग की। कुल मिलाकर हिंदी को कमजोर करने के प्रयास होते रहे।
2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद एक बार फिर इस विषय पर गहन-मंथन हुआ। सरकार ने हिंदी के साथ-साथ सभी भाषाओं को समान महत्व देने का निर्णय किया। नई शिक्षा नीति 2020 में भी भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया। नई शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष और इसरो के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय कस्तूरीरंगन ने रेखांकित किया कि अपनी भाषा में कोई भी व्यक्ति बेहतर तरीके से सीख और समझ सकता है। इसलिए नई शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में, विशेषकर, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि इस राह में अभी भी अनेक बाधाएं हैं। नई शिक्षा नीति में यहां पहले के मुकाबले अधिक लचीली भाषा नीति अपनाई गई। इस नीति में कोई भी भाषा अनिवार्य न करते हुए कोई दो भारतीय भाषाएं और कोई अन्य भाषा पढ़ने की बात कही गई। अब हिंदी या कोई भी भाषा थोपने की बात नहीं है और विद्यार्थी अपना हित सोचते हुए स्वेच्छा से भाषाएं चुन सकते हैं। नई शिक्षा नीति में भाषा शिक्षण की स्वतंत्रता के बावजूद भी राजनीतिक विरोध हुआ। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता का इस तरह की बातों से कोई खास सरोकार नहीं रहा। आम व्यक्ति केवल अपनी सुविधा देखता है। वह अच्छी तरह जानता है कि अपने प्रदेश में उसे अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा आनी चाहिए, देश भर में संपर्क के लिए हिंदी को अपनाना चाहिए और विदेशों से संपर्क अथवा वहां की ज्ञान-विज्ञान को समझने के लिए अंग्रेजी भी आनी चाहिए। इसलिए यह विरोध कहीं भी सामान्य जन का न था और न है, यह केवल राजनीतिक है।
भाषा-नीति के संबंध में मैं यहां मैं एक और वैचारिक समानता का उल्लेख करना चाहूंगा। यह वैचारिक समानता महात्मा गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच साफ दिखाई देती है। महात्मा गांधी मातृभाषा में शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रबल पक्षधर थे, जिसे वे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारते थे। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी कहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के लिए हमें अपनी किसी भाषा को तो अपनाना होगा, जो विदेशी न हो। निश्चय ही व्यवहारिक स्तर पर, वह हिंदी के अलावा कोई और भाषा नहीं हो सकती। मैं यहां मोहनदास कर्मचंद गांधी और मोहन भागवत के विचारों में कोई अंतर नहीं देखता।
2014 के पश्चात जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि भाषा की राजनीति और उसके नाम पर देशवासियों के बीच पैदा की जा रही दरार को पाटने के लिए भारत की सभी भाषाओं को समान महत्व देने का निर्णय किया गया। इस संबंध में दो निर्णय नई शिक्षा नीति में दिखाई देते हैं, पहला मातृभाषा में शिक्षा और कोई भी दो भारतीय भाषाएं पढ़ने की छूट। इसमें कहीं भी हिंदी या किसी अन्य भाषा की अनिवार्यता की बात नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत की सभी भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं। यहां भी किसी भाषा को प्रधानता देने की बात नहीं है।
पिछले वर्ष हिंदी दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग में भारतीय भाषा अनुभाग के गठन की घोषणा की, जिसमें विभिन्न भाषाओं के अधिकारी रखे गए हैं। उनके द्वारा यह घोषणा भी की गई है कि उनके मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को पत्रादि जल्द ही उनकी भाषाओं में भेजे जाएंगे। इसी प्रकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर 2021 को एक उच्च-प्राधिकारी समिति के रूप में भारतीय भाषा समिति की आधिकारिक स्थापना की गई। इस समिति की भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में वर्णित भारतीय भाषाओं के समग्र विकास की दिशा में सुझाव देना और नई शिक्षा नीति के अनुरूप भाषाओं का समग्र विकास ताकि भारतीय भाषाओं को शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में पुनर्जीवित करना है। जिसके अंतर्गत भाषा संस्थानों, भाषाविदों और भाषाओं का डेटा बैंक बनाना, भारतीय भाषाओं के लिए विशिष्ट कार्य योजनाओं का निर्माण, शोध, तकनीकी, व्यापार और भारतीय ज्ञान प्रणाली में भाषा के अनुप्रयोग आदि हैं। साथ ही समिति को 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकों का निर्माण का कार्य भी कर रही है। समिति के माध्यम से देश की 22 भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में अनुवाद के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर -अनुवादिनी- भी तैयार किया गया है।
वर्तमान सरकार न्यायपालिका में सभी स्तरों पर राज्यों की मांग के अनुसार उनकी भाषा में न्याय देने के लिए प्रयासरत है। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2019 में कृत्रिम मेधा आधारित अनुवाद प्रणाली (एसयूवीएसएस- सुवास) की मदद से निर्णयों का अनुवाद 13 भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है। यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भारतीय भाषाओं में निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालयों में फैसलों के डिजिटल रिकॉर्ड और अनुवाद के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी विकसित किया गया है। इससे निर्णयों के हिंदी/क्षेत्रीय भाषा अनुवाद जनता के लिए आसान पहुंच में आ सकें। उल्लेखनीय है कि 2023 में प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि नागरिकों को उनकी मातृभाषा में न्याय मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) और सुवास के जरिए सुप्रीम कोर्ट के हजारों फैसले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनका उद्देश्य 2026 तक इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों की पुस्तकें 12 भारतीय भाषाओं में तैयार और उपलब्ध करवाना है। पहले और दूसरे वर्ष के लिए अब तक लगभग 600 पुस्तकें 12 भाषाओं में तैयार और अपलोड कर दी गई हैं और इस दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में लगभग 22,000 पाठ्य-पुस्तकें और स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 4000–5000 पुस्तकें तैयार करने की योजना है। मध्यप्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों में राज्य की राजभाषा हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रारंभ की है। लेकिन यहां यह भी विचारणीय है कि जब तक भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्वभाषा माध्यम से रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होंगे वे भारतीय-भाषा माध्यम अपनाने से हिचकेंगे। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
इस तरह अब संघ सरकार की भाषा नीति राजभाषा से आगे निकलकर सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय-भाषाओं की पहचान देते हुए आगे बढ़ाने की है। शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग व प्रसार बढ़ाने तथा उनमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। निश्चय ही यह नीति भारत की सामासिक एकता को आगे बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण-प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने व देश के सर्वांगीण विकास में कारगर सिद्ध होगी।
(लेखक गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग के पूर्व क्षेत्रीय उपनिदेशक और वैश्विक हिंदी सम्मेलन के संस्थापक एवं निदेशक हैं)
#हिंदीदिवस, #HindiDiwas, #हिंदीकीनीति, #भारतीयभाषाएं, #स्वतंत्रतासंग्राम, #HindiPolitics, #हिंदीऔरभारत, #IndianLanguages, #LanguagePolicy





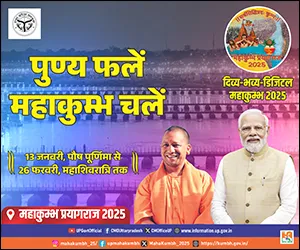
4.jpg)
4.jpg)
4.jpg)
4.jpg)
4.jpg)
